Hello friends, welcome to our website, so today we are telling you about the Indus Valley Civilization in this post, first of all, what is the Indus Valley Civilization, what is the history of the Indus Valley Civilization, the chronology of the Indus Valley Civilization, architecture, social What is life, political system, then read the post completely for information about all these. In this post, you will get complete information related to Indus Valley Civilization. So read the post completely..|
हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी वेबसाइट पर तो आज हम आपको इस पोस्ट में सिन्धु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहे है तो सबसे पहले बात करेंगे सिन्धु घाटी सभ्यता क्या है सिन्धु घाटी सभ्यता का इतिहास क्या है सिन्धु घाटी सभ्यता का कालक्रम,स्थापत्य,सामाजिक जीवन, राजनितिक व्यवस्था क्या है तो इन सब की जानकारी के लिए POST को पूरा पढिये इस पोस्ट में आपको सिन्धु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरी जानकरी मिलेगी. तो पोस्ट को पूरा पढिये..|
Table of Contents
सिन्धु घाटी सभ्यता | Sindhu Ghaati Sabhyta In Hindi
सिन्धु-सरस्वती सभ्यता
भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में विकसित हुई यह सभ्यता सिन्धु तथा सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई अतः इसे सिन्धु-सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में सरस्वती नदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी के तट पर वेदों की रचना हुई है। वेदों तथा वैदिक साहित्य, महाकाव्यों, पुराणों आदि में इसका व्यापक विवरण प्राप्त होता है।
सरस्वती नदी को सिन्धु नदी सहित छ नदियों की माता माना है। अतः सरस्वती नदी सिन्धु नदी से भी प्राचीन है। अतः सरस्वती नदी सभ्यता, सिन्धु घाटी से पूर्व की एक सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित सभ्यता थी। वास्तव में वैदिक संस्कृति का जन्म और विकास इसी नदी के तट पर हुआ था। यह अब स्पष्ट हो गया कि सरस्वती नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकल कर आदि बद्री में पहुँचती है। वहाँ से हरियाणा, राजस्थान होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती थी। इसके लुप्त होने के बारे में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं।
भौगोलिक विस्तार -
1921 में दयाराम साहनी, तथा 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा हडप्पा तथा मोहनजोदडो में किए गए उत्खनूनों से सिन्धु-सरस्वती सभ्यता का अनावरण हुआ। वर्तमान में इस सभ्यता के पुरास्थल हमें पाकिस्तान में सिन्ध, पंजाब एवं बलूचिस्तान प्रान्तों से तथा भारत में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र प्रान्तों से मिले हैं।
इन सभी प्रान्तों से प्राप्त पुरास्थलों की सूची निम्नलिखित है-
- बलूचिस्तान (पाकिस्तान) - सुत्कागेण्डोर, सुत्काकोह बालाकोट
- पंजाब (पाकिस्तान) - हडप्पा, जलीलपुर, रहमान ढेरी, सराय खोला, गनेरीवाल
- सिंघ (पाकिस्तान) - मोहनजोदूडो, चन्हुदंडो, कोटदीजी, जुदीरजोदडो
- पंजाब (भारत) - रोपड कोटला निहंगखान ,संघोल
- हरियाणा (भारत) - बणावली, मीताथल, राखीगढ़
- जम्मू-कश्मीर (भारत) - माण्डा (जम्मू)
- राजस्थान (भारत) - कालीबंगा
- उत्तर प्रदेश (भारत) - आलमगीरपुर (मेरठ) हुलास (सहारनपुर)
- गुजरात (भारत) - रंगपुर, लोथल, प्रभासपाटन, रोजदी. देशलपुर, सुरकोटडा, मालवण, भगतराव, धौलावीरा
- महाराष्ट्र (भारत) - दैमाबाद (अहमदनगर)
नवीन परिगणना के हिसाब से सिन्धु-सरस्वती सभ्यता के लगभग 1400 स्थल हमें ज्ञात हैं। जिनमें 917 भारत में 481 पाकिस्तान में तथा शेष 2 स्थल अफगानिस्तान (शोर्तुगोई मुड़ीगाक) में हैं।
सिन्धु-सरस्वती सभ्यता के विस्तार की उत्तरी सीमा जम्मू क्षेत्र में चेनाब नदी के किनारे स्थित माण्डा पुरास्थल है। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद (अहमदनगर) नामक स्थल पर है। यमुना नदी की सहायक हिण्डन नदी के तट पर स्थित, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी पुंरास्थल है तथा सबसे पश्चिमी पुरास्थल बलूचिस्तान में मकरान तट पर स्थित सुत्कागेण्डोर, है। अर्थात् सिन्धु सभ्यता पश्चिम से पूर्व तक 1600 कि.मी. तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 कि.मी. में फैली हुई थी। सिन्धु सभ्यता का वर्तमान में प्राप्त भौगोलिक विस्तार लगभग 15- लाख वर्ग किमी. है।
सिन्धु-सरस्वती सभ्यता का कालक्रम -
सिन्धु-सरस्वती विद्वान एक मत नहीं है । सभ्यता के कालक्रम को लेकर अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदडो के अन्तिम चरण को 2500 ई.पू. में निर्धारित करते हुए प्रारम्भ 2800 ई.पू. माना है। मार्टीमर व्हीलर ने इस सभ्यता की तिथि 2500 ई.पू. से 1500 ई. पू. के मध्य मानी है। रेडियो-कार्बन पद्धति से इस सभ्यता की तिथि 2300-1750 ई.पू. मानी गई हैं। लेकिन नवीन उत्खननों तथा अनुसंधानो से सिन्धु-सरस्वती सभ्यता के नवीन तथ्य. प्रकाश में आये हैं। इन नवीन उत्खननों से पता चलता हैं कि यह सभ्यता 5000 ई. पू. से 3000 ई. पू. के मध्य की हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता हैं कि सिन्धु-सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता थी।
नगर नियोजन तथा स्थापत्य -
सुनियोजित नगरों का निर्माण सिन्धु-सरस्वती सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। प्रत्येक नगर के पश्चिम में ईटों से बने एक चबूतरे पर गढी' या दुर्ग का भाग है और इसके पूर्व की ओर अपेक्षाकृत नीचे धरातल पर नगर भाग प्राप्त होता है जो जन सामान्य द्वारा निवासित होता था। गढ़ी वाला भाग शायद पुरोहितों अथवा शासक का निवास स्थान होता था। गढी के चारों ओर परकोटे जैसी दीवार थी।
नगरों की सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखती हैं। जिससे सम्पूर्ण नगर वर्गाकार या आयताकार खण्डों में विभक्त हो जाता है। सिन्धु-सरस्वती सभ्यता कालीन सड़कें पर्याप्त चौड़ी होती थीं, इनकी चौड़ाई 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है और कभी-कभी ये सड़कें आधे मील की लम्बाई तक मिली हैं।
भवन विभिन्न आकार-प्रकार के हैं जिनकी पहचान धनाढ्यों के विशाल भवन, सामान्य जनों के साधारण घर, दुकानें, सार्वजनिक भवन आदि के रूप में की जा सकती है। साधारणतया घर पर्याप्त बड़े थे और उनके मध्य में आँगन होता था। आँगन के एक कोने में ही भोजन बनाने का प्रबन्ध था। और इर्द-गिर्द चार या पाँच कमरे बने होते थे। प्रत्येक घर में स्नानागार और पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबन्ध था और घरों में कुएँ भी थे। यह उल्लेखनीय है कि सिन्धु -सरस्वती सभ्यता के लोग सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करते थे।
गलियाँ 1 से 2.2 मीटर तक चौड़ी थी। ये गलियाँ सीधी होती थी। मोहनजोदडो की हर गली में एक सार्वजनिक कूप मिलता है। कालीबंगा में गलियों एवं सड़कों को एक आनुपातिक ढंग से निर्मित किया गया था। गलियाँ वहाँ 1.8 मी, चौड़ी और मुख्य सड़कें एवं राजमार्ग इससे दुगुने (3.6 मी.) तिगुने (5.4 मी.) या चौगुने (7.2 मी.) चौड़े थे।
सिन्धु-सरस्वती सभ्यता के भवनों में पकाई गई ईटों का इस्तेमाल होना एक अद्भुत बात है। जिस समय अन्य सभ्यताएँ पक्की ईंटों से अनभिज्ञ थी उस समय सिन्धु सरस्वती सभ्यता के लोग बड़ी कुशलता से उनका प्रयोग कर रहे थे। निर्माण में प्रयुक्त ईंटों का अनुपात 4:2: 1 था।
जल निकास प्रणाली -
जल प्रबन्धन एवं जल निकास व्यवस्था सिन्धु-सरस्वती व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी। लगभग प्रत्येक बड़े घर में कुएँ की व्यवस्था थी। सार्वजनिक उपयोग हेतु भी कुछ कुए गलियों के किनारे खुदाये गये थे। जल उपलब्धि के साथ ही जल निकासी हेतु भी व्यवस्थित प्रणाली थी। प्रायः प्रत्येक घर के किनारे वर्षा एवं घर के अनुपयुक्त पानी की निकासी हेतु नालियाँ थी। प्रत्येक घर की नाली गली की प्रमुख नालियों से होकर मुख्य सड़क की नालियों में गिरती थी। पक्की ईंटों से निर्मित नालियाँ अधिकांशतः ढकी हुई होती थी।
नालियों के बीच-बीच में थोड़ी दूरी पर गड्ढे बनाये जाते थे जिनमें अवरोधक कूड़ा-कचरा गिर जाता था। और जल निकास के बहाव में रूकावट नहीं होती थी। इन गड्ढों के ढक्कन हटाकर सफाई की जाती थी। ऊपरी मंजिलों का पानी पक्की ईंटों से बने पटावनुमा नाली से नीचे गिरता था। कालीबंगा में लकड़ी के खोखले तूनों का उपयोग नालियों के रूप में किया जाता था। कहीं पर भी पानी का जमाव या गंदा पानी भरा नहीं रहता था। सिन्धु -सरस्वती सभ्यता नगरीय स्वच्छता का श्रेष्ठतम प्रतीक है। ऐसी नाली व्यवस्था विश्व मे अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होती। यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठतम मान्य शहर पेरिस में भी ऐसी जल निकासी व्यवस्था नहीं थी।
विशिष्ट भवनों का स्थापत्य -
विशाल स्नानागार - यह मोहनजोदडो में स्थित सबसे महत्वपूर्ण व भव्य निर्माण का नमूना है। यह स्नानागार 39 फीट लम्बा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इस कुण्ड में जाने के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें ईंटों की चिनाई बड़ी सावधानी एवं कुशलता के साथ की गई है। स्नान कुण्ड की फर्श का ढाल दक्षिण-पश्चिम की ओर है। स्नानागारके दक्षिणी-पश्चिमी कोने में ही एक महत्वपूर्ण नाली थी जिसके द्वारा पानी निकास की व्यवस्था थी। इस स्नानागार का उपयोग धार्मिक उत्सवों तथा समारोहो पर होता होगा।
विशाल अन्नागार - हडप्पा के गढी वाले क्षेत्र में एक विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। यह ऊँचे चबूतरे पर बना हुआ था जिसके पीछ बाढ़ से बचाव तथा सीलन से बचाने का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। यह अन्नागार या भण्डारागार कई खण्डों में विभक्त था और हवा आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था थी। यह अन्नागार राजकीय था। हडप्पा के अतिरिक्त हमें मोहनजोदडो एवं राखीगढी से भी अन्नागारों के अवशेष मिले हैं
गोदी या बंदरगाह (लोथल) - लोथल में पक्की ईटों का एक गोदी या बंदरगाह (डॉकयार्ड) मिला है। जिसका औसत आकार 214.36 मीटर है। इसकी वर्तमान गहराई 3.3 मीटर है। अनुमानतः इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिसमें से जहाज आते जाते थे। लोथल का डॉकयार्ड वर्तमान में विशाखापट्टनम् में बने हुए डॉकयार्ड से बड़ा है। इनके अतिरिक्त धौलावीरा का जलाशय तथा विशाल स्टेडियम भी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से प्राप्त नमूनों में विशिष्ट स्थान रखते हैं।
सामाजिक जीवन -
वर्गीकरण - समाज में कई वर्ग थे। यहाँ सुनार, कुम्भकार, बढई, दस्तकार, जुलाहे, ईंटें तथा मनके बनाने वाले पेशेवर लोग थे। कुछ विद्वानों के अनुसार उस काल में पुरोहितों तथा अधिकारियों व राजकर्मचारियों का एक विशिष्ट वर्ग रहा होगा। सम्पन्नता की दृष्टि से गढ़ी वाले क्षेत्र के लोग सम्पन्न रहे होंगे तथा निचले नगर में सामान्य लोग रहते होंगे।
परिवार तथा स्त्रियों की स्थिति - खुदाई में मिले भवनों से साफ पता लगता है कि सिन्धु-सरस्वती सभ्यता काल में पृथक्-पृथक् परिवारों के रहने की योजना दिखाई देती है। अतः इस काल में एकल परिवार योजना रही होगी। इस सभ्यता में भारी संख्या में नारियो की मूर्तिया मिली हैं। संभवतः यहाँ नारियों का स्थान सम्मानजनक था। क्रीट तथा अन्य भूमध्य सागरीय सभ्यताओं में (मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता था। अतः इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि सिन्धु-सरस्वती सभ्यता में भी मातृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन रहा होगा। ऐसी स्थिति में स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा।
खान-पान - सिन्धु–सरस्वती सभ्यता के वासी अपने भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, दूध, फल, माँस आदि का सेवन करते थे। फलो में वे अनार, नारियल, नींबू, खरबूजा, तरबूज आदि से परिचित थे। पशु पक्षियों की कटी-फटी हड्डियों के मिलने से उनके मांसाहार का पता चलता है। भेड, बकरी, सुअर, मुर्गा, बत्तख, कछुआ आदि का मांस खाया जाता था। अनाज तथा मसाले पीसने के लिए सिल-बट्टे का प्रयोग किया जाता था।
रहन-सहन, आमोद-प्रमोद - स्त्रियों की मृणमूर्तियों से उनकी वेशभूषा की जानकारी मिलती है। इन मूर्तियों में उनके शरीर का ऊपरी भाग वस्त्रहीन है तथा कमर के नीचे घाघरे जैसा एक वस्त्र पहना हुआ है। कुछ मूर्तियों में स्त्रियों को सिर के ऊपर एक विशेष प्रकार के पंखे की आकृति का परिधान पहने हुए दिखाया गया है। पुरूषों की अधिकांश आकृतियाँ बिना वस्त्रों के हैं। हालांकि पुरूष कमर पर एक वस्त्र बाँधते थे। कुछ स्थानों पर पुरूषों को शाल ओढे हुए दिखाया गया है।
पुरुषों में कुछ लोग दाढी-मूँछ रखते थे तथा हजामत करते थे। स्त्रियाँ अपने केशों का विशेष ध्यान रखती थी। बालों को संवारने के लिए कंधियों का और मुख छवि देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता था। खुदाई में कांसे में बने हुए दर्पण एवं हाथीदांत की कंघियाँ प्राप्त हुई हैं। स्त्री-पुरूष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। मुख्य रूप से मस्तकाभूषण, कण्ठहार. कुण्डल, अगूठियाँ, चूडियाँ, कटिबन्ध, पाजेब आदि पहने जाते थे।
सिन्धु सरस्वती सभ्यता के क्षेत्र की खुदाई में मिट्टी के कई खिलौने मिले हैं। इसके अतिरिक्त पासे भी मिले हैं जिससे पासों के खेलों जैसे चौसर का प्रमाण मिलता है। नर्तकी की प्राप्त मूर्ति से नृत्य संगीत का पता लगता है। कुछ मुहरों पर सारंगी और वीणा का भी अंकन है।
आर्थिक जीवन -
कृषि - सिन्धु-सरस्वती सभ्यता के पर्याप्त जनसंख्या वाले महानगरों का उदय एक अत्यन्त उपजाऊ प्रदेश की पृष्ठभूमि में ही सम्भव था। अधिकांश नगर सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा से युक्त उपजाऊ नदी के तटों पर स्थित थे। जलवायु की अनुकूलता, भूमि की उर्वरता एवं सिंचाई की सुविधाओं के अनुरूप विभिन्न स्थलों पर फसलें उगाई जाती थी।
गेहूँ के उत्पादन के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। हडप्पा.. (और मोहनजोदड) से जी के भी प्रमाण मिले हैं। ऐसा जान पड़ता है कि गेहूँ और जो इस सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न थे। इसके अतिरिक्त खजूर, सरसों, तिल, मटर तथा राई और चावल से भी परिचित थे। कपास की खेती होती थी और वस्त्र निर्माण एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा होगा। सिन्धु-सरस्वती सभ्यता में ही (कपास की खेती का विश्व को पहला उदाहरण.. मिला है। सिन्धु क्षेत्र में उपज होने के कारण यूनानियों ने कपास के लिए (सिन्डन" शब्द का प्रयोग किया। यहाँ की उर्वरता का मुख्य कारण सिन्धु तथा सरस्वती नदियों में आने वाली बाढ़ थी जो कि काफी जलोढ मिट्टी लाकर मैदानों में छोड़ देती थी। सम्भवतः खेतों को जोतने के लिए हलों का प्रयोग होता था। कालीबंगा में जुते हुऐ खेत का प्रमाण मिला है।
पशुपालन - गाय, बैल, भैंस, भेड़ पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे। बकरी तथा सुअर भी पाले जाते थे। कुत्ते, बिल्ली तथा अन्य पशु भी पाले जाते होंगे। हाथी और ऊँट की हड्डियाँ बहुत कम मिली हैं लेकिन मुहरों पर इनका अंकन विपुल है। सिन्धु सभ्यता के निवासी घोडे से भी परिचित थे लोथल से घोड़े की तीन मृण मूर्तियाँ तथा एक जबडा मिला है, जो घोड़े का है।
उद्योग तथा शिल्प - सिन्धु-सरस्वती सभ्यता करिययुगीन सभ्यता है। ताँबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ताम्र और कांस्य के सुन्दर बरतन हड़प्पा कालीन धातु कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं।
ताँबे से निर्मित औजारों में उस्तरे, छैनी हथौड़ी, कुल्हाडी, चाकू, तलवार आदि मिली है। कांस्य की वस्तुओं के
उदाहरण में निर्तकी की मूर्ति मुख्य है। सिन्धु सभ्यता में सोने तथा चाँदी का भी प्रयोग होता था तथा यहाँ के लोग मिट्टी के बरतन बनाने की कला में भी प्रवीण थे। मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। चन्हदड़ो तथा लोथल में मनका बनाने वालों की पूरी कर्मशाला मिली है। मनके सोने-चाँदी, सेलखडी, सीप तथा मिट्टी से बनाये जाते थे। लोथल तथा बालाकोट से विकसित सीप उद्योग के प्रमाण मिले हैं। सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई के धन्धे भी अत्यन्त विकसित रहे होंगे।
व्यापार एवं वाणिज्य - सिन्धु-सरस्वती सभ्यता में आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार अत्यन्त विकसित अवस्था में था। उद्योग-धन्धों के लिए कच्चा माल राजस्थान, गुजरात, सिन्ध, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान तथा मेसोपोटामिया से मँगाया जाता था। राजस्थान से ताँबा तथा सोना मैसूर से आता था। यहाँ के लोगों के मेसोपोटामिया से व्यापारिक सम्बन्ध होने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। मेसोपोटामिया से सिन्धु सरस्वती सभ्यता की कई दर्जन मुहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में दिलमन सगान और मेलुहा नामक स्थानों की चर्चा की गई है। जिनके साथ वहाँ के लोगो के व्यापारिक सम्बन्ध थे। मेलुहा शब्द भारत के लिए प्रयुक्त किया गया माना जाता सिन्धु-सरस्वती सभ्यता में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली/का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से भारी- संख्या में मुहरें मिली है लेकिन उनका उपयोग पत्र या पार्सल पर छाप लगाने के लिए किया जाता था। माप-तौल का एक निश्चित क्रम था। तोल की ईकाई 16 के अनुपात में थी जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 320 सोलह के अनुपात में तौल मापने की परम्परा हमारे यहाँ आधुनिक काल तक चलती आ रही है।
धार्मिक जीवन - सिन्धु सरस्वती सभ्यता का प्राचीन धर्म के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया जाता है। मातृदेवी की उपासना, पशुपति शिव की परिकल्पना, मूर्तिपूजा, वृक्षपूजा, अग्निपूजा, जल की पवित्रता, तप एवं योग की परम्परा उनके धर्म की ऐसी विशेषताएँ है जिनकी निरन्तरता हमारे वर्तमान धार्मिक जीवन में देखी जा सकती है बणावली से प्राप्त एक अर्द्धवृत्ताकार ढाँचे के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों ने मंदिर होने की संभावना व्यक्त की है।
मातृदेवी की उपासना - हड़प्पा, मोहनजोदडो एवं चुन्हदडो से विपुल मात्रा मे मिट्टी की बनी हुई तारी-मूर्तियाँ मिली हैं, जिन्हें पूजा के लिए निर्मित मातृदेवी की मूर्तियाँ माना गया है। भारत में देवी पूजा या शक्ति पूजा की प्राचीनता का प्रारम्भिक बिन्दु सिन्धु-सरस्वती सभ्यता में देखा जा सकता है।
सिन्धु-सरस्वती सभ्यता से प्राप्त मुहरों के कुछ चित्रों से भी मातृदेवी की उपासना के संकेत मिलते हैं। राखीगढ़ी में हमें बहुत से अग्निकुण्ड एवं अग्नि वेदिकायें) (संभवतः यज्ञवेदियाँ) मिली हैं। इन क्षेत्रों में धार्मिक यज्ञों या अग्निपूजा का प्रचलन रहा होगा।
देवता (शिव) की उपासना- जॉन मार्शल ने मोहनजोदडो की एक मुहर पर अंकित देवता को ऐतिहासिक काल के पशुपति शिव का प्राक रूप माना है। इस मुहर में देवता को त्रिमुख एवं पदमासन मुद्रा में बैठे हुए, दिखाया गया है। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केन्द्रित लगती हाथी, एक चीता, एक भैंसा तथा एक है, इसके चारों ओर एक (गैंडा एवं आसन के नीचे हरिण अंकित है। इस अंकन में शिव के तीन रूप देखे जा सकते हैं। जो निम्न है- (1) शिव का त्रिमुख रूप (2) पशुपति रूप (3) योगेश्वर रूप
अग्निवेदिकाएँ - कालीबंगा लोथल बणावली एवं राखीगढ़ी के उत्खननों से हमें अनेक अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। कुछ स्थलों पर उनके साथ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिनसे उनके धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने की संभावना प्रतीत होती है। बणावली एवं राखीगढ़ी से वृत्ताकार अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, जिन्हें अर्द्धवृत्ताकार ढाँचे के मन्दिर या घेरे में संयोजित किया गया है।
पशु पूजा, वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा - कई मुहरों पर एक श्रृंग वृषभ (एक सींग वाले बैल) का अंकन मिलता जिसके सामने. सम्भावत: धूपदण्ड रखा हुआ है।
अनेक छोटी-छोटी मुहरों पर वृक्षों के चित्रांकन से वृक्ष पूजा का आभास होता है। कई छोटी मुहरों पर एक वृक्ष के चारों ओर छोटी दीवार या वेदिका बनी मिलती है। जो उनकी पवित्रता तथा पूजा–विषय होने की द्योतक है। कुछ मुहरों पर स्वास्तिक चक्र एवं क्रॉस जैसे मंगलचिन्हों का भी अंकन काफी संख्या में मिलता है।
सिन्धु-सरस्वती सभ्यता के अवशेषों से जल की पवित्रता एवं धार्मिक स्नान की परम्परा के संकेत भी मिलते है। यह अनुमान किया जाता है कि मिट्टी और ताँबे से बनी कुछ गुटिकाओं का ताबीजों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मनके भी जैसे त्रिपत्र-अलंकरण युक्त होते थे जो "ताबीज या रक्षाकवच के रूप में काम आते होंगे।
योग एवं साधना की परम्परा - विद्वानों का अनुमान है कि सिन्धु-सरस्वती सभ्यता में योग एवं साधना की परम्परा के अस्तित्व का संकेत भी मिलता है। इसके दो साक्ष्य हैं – (1) पशुपति मुहर में पदमासन मुद्रा में बैठे योगेश्वर शिव का अंकन (2) मोहनजोदडो से प्राप्त 'योगी' की मूर्ति जिसकी दृष्टि नासाग्र पर टिकी है।
मृतक संस्कार एवं पुनर्जन्म में विश्वास- मार्शल के अनुसार इस सभ्यता के लोग तीन प्रकार से शवों का क्रिया कर्म करते थे (1) पूर्ण समाधिकरण इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण शव को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था। (2) आंशिक समाधिकरण इसके अन्तर्गत पशु-पक्षियों के खाने के पश्चात् शव के बचे हुए भाग गांड़े जाते थे। (3) दाहकर्म- इसमें शव जला दिया जाता था और कभी-कभी भस्म गाड़ दी जाती थी। शव के साथ कभी-कभी विविध आभूषण, अस्त्र-शस्त्र पात्रादि भी रखे मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वे पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे।
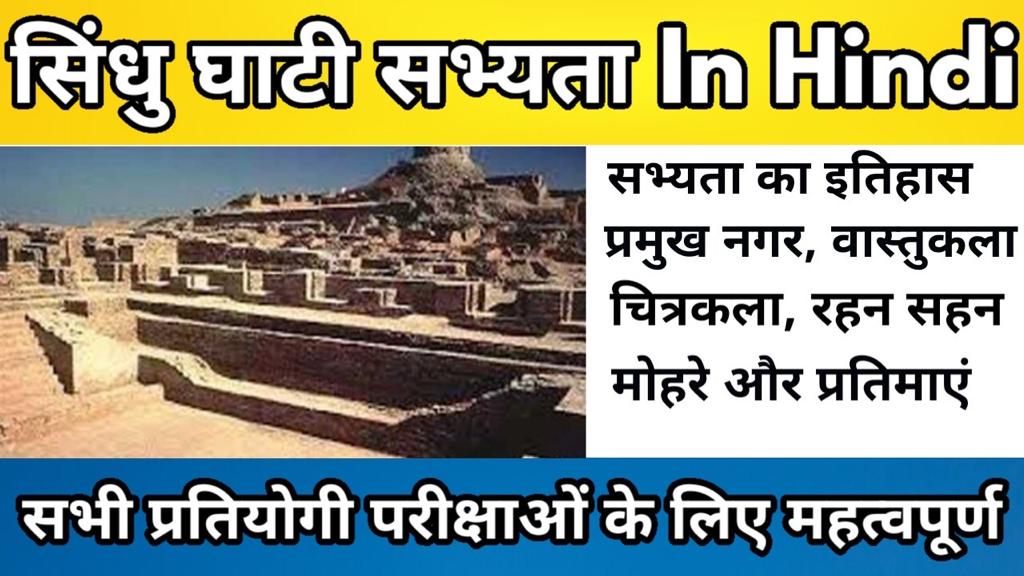
राजनीतिक व्यवस्था
सिन्धु-सरस्वती सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है (व्हीलर और पिगट का) मानना है कि हडप्पा एवं मोहनजोदडो में दक्षिणी मेसोपोटामिया की तरह पुरोहित का शासन था। कुछ अन्य विद्वान इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इस सभ्यता के नगरों में मिश्र एवं मेसोपोटामिया की तरह कोई मन्दिर नहीं मिला है। सिन्धु सभ्यता के वासियों की मूल रूचियाँ व्यापार मूलक थी, और उनके नगरों में सम्भवतः व्यापारी वर्ग का शासन था।
किंतु नगर-नियोजन, पात्र - परम्परा, उपकरण निर्माण, बाट एवं माप आदि के संदर्भ में मानकीकरण एवं समरूपता किसी प्रभावी राजसत्ता के पूर्णं एवं कुशल नियन्त्रण के प्रमाण हैं। व्हीलर के अनुसार यह साम्राज्य, जो इतनी दूर तक फैला हुआ था, एक अच्छे प्रकार से शासित साम्राज्य था। इतने बड़े साम्राज्य के चार प्रमुख क्षेत्रीय केन्द्र रहे होंगे - हडप्पा, मोहनजोदडो, कालीबंगा और लोथल। सिन्धु-सरस्वती सभ्यता के निवासियों का जीवन शान्तिप्रिय था। युद्ध के अस्त्र-शस्त्र बहुत अधिक संख्या में नहीं मिलते हैं। उपलब्ध हथियारों में काँसे की आरी, ताँबे की तलवारें, कांस्य के बने भालों के अग्रभाग, कटारें, चाकू, नोकदार बाणाग्र आदि मिलते हैं।
कला
सिन्धु सरस्वती सभ्यता की मुहरें, मूर्तियाँ, मृद्भाण्ड, मनके एवं धातु से बनी कतिपय वस्तुयें कलात्मक उत्कृष्टता एवं समृद्धि की परिचायक हैं।
मूर्तिकला - मोहनजोदडो से प्राप्त उल्लेखनीय पत्थर की एक खंडित मानव-मूर्ति जिसका सिर से वक्षस्थल तक का ही भाग बचा है, उल्लेखनीय है। यह मूर्ति त्रिफूलिया आकृति से युक्त शाल ओढे हुए है। हडप्पा के उत्खननों से पत्थर की दो मूर्तियाँ) उपलब्ध हुई हैं। कला के क्षेत्र में शैली और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से ये काफी हद तक यूनानी कलाकृतियों के समकक्ष रखी जा सकती हैं। इनमें से एक लाल बलुआ पत्थर का धड़ है। यह एक युवा पुरूष का धड़ है और इसकी रचना में कलाकार ने मानव शरीर के विभिन्न अंगों के सूक्ष्म अध्ययन का प्रमाण दिया है। दूसरी सलेटी चूना पत्थर की नृत्यमुद्रा में बनाई गई आकृति का धड़ है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों का विन्यास आकर्षक है। यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि यह नृत्यरत नटराज की मूर्ति है। कांस्य मूर्तियों में सर्वाधिक कलात्मक नर्तकी की मूर्ति है। यह मूर्ति 14 सेमी ऊँची है। इस मूर्ति में नारी के अंगों का न्यास सुन्दर रूप से हुआ है। इस मूर्ति का निर्माण द्रवीय मोम विधि से हुआ है।
कांस्य मूर्तियों में दैमाबाद से प्राप्त एक रथ की मूर्ति अत्यन्त आकर्षक है। एम. के. धवलिकर के शब्दों में दैमाबाद से प्राप्त उपर्युक्त चारों कांस्य-मूर्तियाँ 'भारतीय प्रागैतिहासिक कला के सम्पूर्ण क्षेत्र में अपनी श्रेणी के श्रेष्ठतम् शिल्प है।" सिन्धु-सरस्वती सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियाँ सर्वाधिक संख्या में मिली हैं। मिट्टी की सर्वत्र सुलभता आकृतियों के निर्माण में धातु एवं पत्थर से अधिक आसानी और कम खर्च के कारण प्रायः सभी प्राचीन संस्कृतियों में मृण्मूर्ति कला लोकप्रिय रही। पाषाण-मूर्तियाँ बहुत कम संख्या में मिली हैं। सिन्धु सभ्यता के विविध क्षेत्रों से उपलब्ध मृण्मूर्तियों के विशाल भण्डार में पशुओं और पक्षियों की मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिली हैं।
मुहरें - मुहरें इस सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं। अधिकांश मुहरों पर किसी न किसी पशु की आकृति एवं सिन्धु लिपि में लेख, जो साधारणतया 3 से 8 अक्षर वाले हैं। अधिकांश मुहरें सेलखडी से निर्मित हैं। ये प्रायः इस सभ्यता के नगर स्थलों से ही मिली हैं। यद्यपि इन मुहरों के निर्माण में एक जैसी सावधानी और कलात्मकता नहीं दिखती, तथापि मुहरों के कुछ सुन्दर उदाहरण विश्व की महान कलाकृतियों में अपना स्थान रखते हैं। मुहरों पर अंकित पशु आकृतियों में सबसे अधिक अंकन कूबड़-विहीन बैल का मिलता है। सिन्धु-सरस्वती सभ्यता में दो मुहरें विशेष उल्लेखनीय हैं। सबसे प्रसिद्ध पशुपति मुहर जिसमें एक चौकी या पीठ पर आसीन 'शिव' एक हाथी, चीता, गैंडा और भैंसें से घिरे हैं। दूसरी मुहर पर एक कुबेड़दार बैल का अंकन है जो मोहनजोदडो से मिली है। सिन्धु-सरस्वती सभ्यता के विविध क्षेत्रों से उपलब्ध मृण मूर्तियों के विशाल भंडार में पशुओं की मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिली हैं।
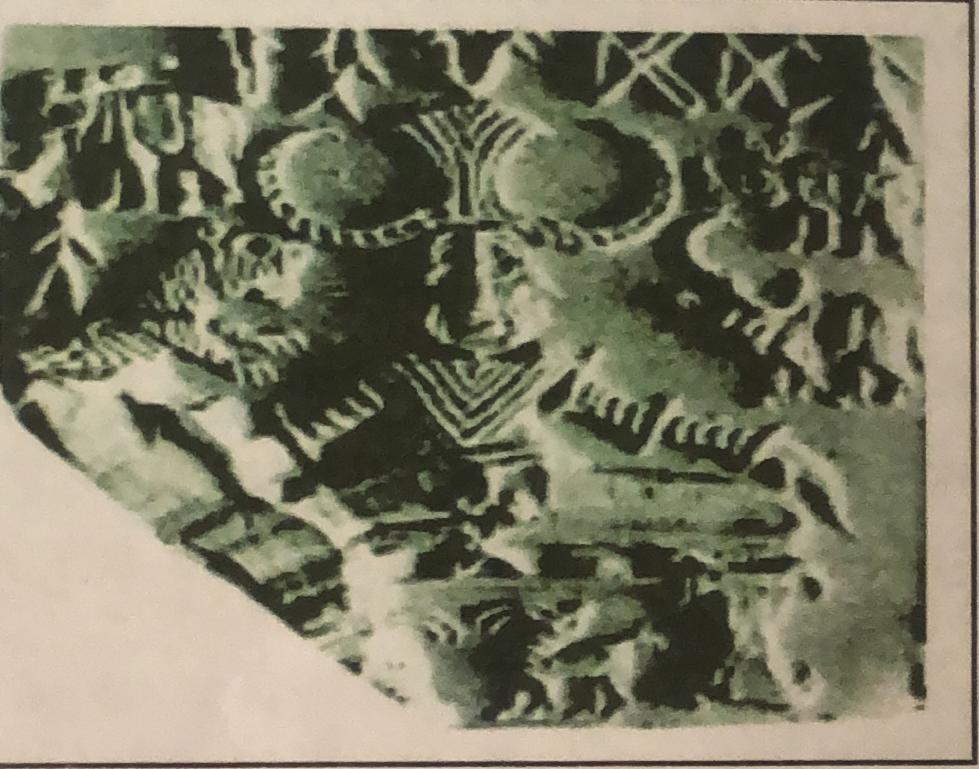
लिपि - सिन्धु-सरस्वती सभ्यता की लिपि अभी भी विद्वानों लिए एक अबूझ रहस्य है। अभी तक इस लिपि को पढ़ने के बारे में 100 से अधिक दावे प्रस्तुत किये जा चुके हैं, लेकिन उन सब की विश्वसनीयता संदिग्ध है। इस सभ्यता में 2500 से अधिक अभिलेख उपलब्ध हैं। सबसे लम्बे अभिलेख में 17 अक्षर येथे प्रायः मुहरों पर मिलते हैं। अभी तक इस लिपि में लगभग 419 चित्रों की पहचान की जा चुकी है। कालीबंगा के एक अभिलेख के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह लिपि दाहिनी ओर से बांयी ओर लिखी जाती थी।
सिन्धु-सरस्वती सभ्यता का निरन्तर सांस्कृतिक प्रवाह - सिन्धु-सरस्वती सभ्यता अपने समय की समृद्ध तथा अनूठी सभ्यता थी। यहाँ के बचे खण्डहर विगत घटना चक्र के मूक लेकिन प्रखर वाचक हैं। यह सभ्यता आज भले ही नष्ट हो गई हो लेकिन उसकी संस्कृति के अनेक तत्वों का अविरल तरंग-प्रवाह हमारी संस्कृति में आज भी विद्यमान है। इस सभ्यता की स्थापत्य कला आज आधुनिक भारत के कई भवनों में दिखाई देती है। वहाँ के नगर नियोजन से प्रेरित कई नगर भारत में विद्यमान हैं। सिन्धु-सरस्वती सभ्यता के निवासियों की आभूषण प्रियता और शृंगार के प्रति जागरूकता हमारे सामाजिक जीवन में आज भी देखी जा सकती है। कृषि तथा पशुपालन में सिन्धु सरस्वती सभ्यता के वासियों ने अनेक नवीन प्रयोग किये जो बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंग बन गये। सिन्धु- सरस्वती सभ्यता का धार्मिक प्रवाह भारतीय संस्कृति में जीवंत रूप में दिखाई देता है। शिव, शक्ति तथा प्रकृति-पूजा सिन्धु-सरस्वती सभ्यता की ही देन है। योग भी इसी सभ्यता की देन है।
Keyword
- सिन्धु घाटी सभ्यता | Sindhu Ghaati Sabhyta In Hindi
- Sindhu Ghaati Sabhyta In Hindi
- Sindhu Ghaati Sabhyta
- Indus Valley Civilization
- सिंधु घाटी सभ्यता pdf
- सिंधु घाटीसिंधु घाटी सभ्यता mcq
- सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए? class 12
- सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है
- सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी कोई दो बिंदु लिखिए
- सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी
- सिंधु घाटी सभ्यता map
- सिंधु घाटी की सभ्यता कब शुरू हुई?
- सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे?
- सिंधु घाटी सभ्यता से आप क्या समझते हैं?
- सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता है?
टिप्पणियाँ(0)